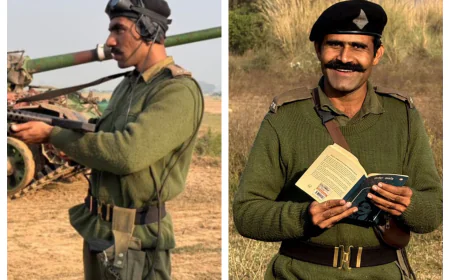एक सामाजिक प्रथा जो महिलाओं को पुनर्विवाह का हक देती है, लेकिन कहीं यह हक़ जबरन सौदेबाज़ी में तो नहीं बदल रहा?
नाता प्रथा'। इस प्रथा के तहत एक विवाहित या विधवा महिला, किसी दूसरे पुरुष के साथ सामाजिक मान्यता के साथ रह सकती है, बशर्ते कि वह पुरुष महिला के पहले पति या उसके परिवार को तयशुदा राशि दे।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आज भी एक अनूठी सामाजिक प्रथा प्रचलित है — 'नाता प्रथा'।
इस प्रथा के तहत एक विवाहित या विधवा महिला, किसी दूसरे पुरुष के साथ सामाजिक मान्यता के साथ रह सकती है, बशर्ते कि वह पुरुष महिला के पहले पति या उसके परिवार को तयशुदा राशि दे। यह रकम 'नाता राशि' कहलाती है।

ऐतिहासिक रूप से, यह प्रथा स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार देने और उसे नए जीवनसाथी के साथ आगे बढ़ने की छूट देने के लिए शुरू हुई थी। उस समय, विधवाओं या छोड़ी गई महिलाओं के लिए समाज में जीना मुश्किल होता था। नाता प्रथा ने उन्हें एक सामाजिक स्वीकार्यता दी।
लेकिन आधुनिक दौर में, यह परंपरा कई जगह अपने मूल उद्देश्य से भटकती दिख रही है। आज कई मामलों में महिलाएं आर्थिक या पारिवारिक दबाव में आकर नाता करने के लिए मजबूर होती हैं। कई बार पुरुषों द्वारा महिलाओं को पैसे के बदले “खरीदने” जैसा व्यवहार भी सामने आता है।

राजसमंद की 28 वर्षीय गीता (बदला हुआ नाम) बताती हैं, "मेरे पहले पति से अनबन हो गई थी। घर वालों ने कहा कि दूसरे आदमी से नाता कर लो, उसने हमारे घर को 1.5 लाख रुपए दिए। मैंने कोई फैसला नहीं लिया था, सब कुछ मेरे परिवार ने किया।" यह कहानी सिर्फ गीता की नहीं, सैकड़ों महिलाओं की है जो आज भी इस प्रथा में अपनी मर्ज़ी के बिना झोंक दी जाती हैं।
कानूनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। भारत का विवाह कानून (Hindu Marriage Act, 1955) 'नाता' को कानूनी विवाह नहीं मानता, इसलिए महिला को बाद में अपने अधिकारों — जैसे कि संपत्ति या गुज़ारा भत्ता — के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
सामाजिक कार्यकर्ता चेतना सिंह कहती हैं, "हम यह नहीं कह रहे कि प्रथा पूरी तरह ग़लत है, लेकिन यह जरूरी है कि इसमें महिला की सहमति, सुरक्षा और अधिकारों की पूरी गारंटी हो।"
नाता प्रथा अपने आप में एक अनूठी सामाजिक सोच का प्रतीक है, जो महिलाओं को दूसरा मौका देती है। लेकिन यदि यह स्वेच्छा की जगह सौदेबाज़ी बन जाए, तो यह महिलाओं की गरिमा और हक़ के ख़िलाफ़ है। अब समय आ गया है कि इस परंपरा का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इसमें सुधार लाए जाएँ ताकि यह वास्तव में स्वतंत्रता का प्रतीक बन सके — शोषण का नहीं।